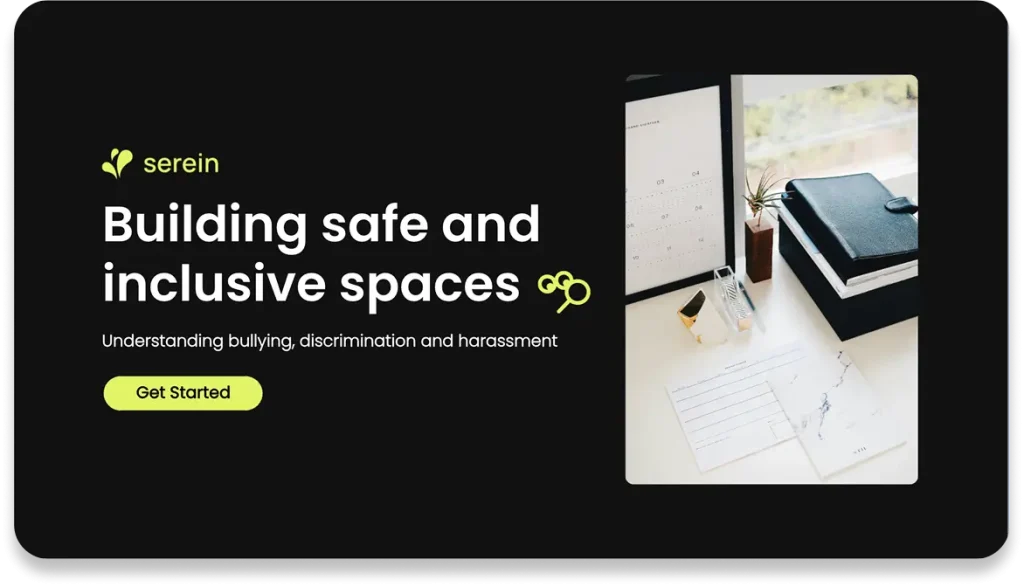‘ना का मतलब ना और जब कोई ना कहता है तो आप रुक जायें.’
2016 मे आई बॉलीवुड की मशहूर फिल्म पिंक में बोली गयी ये पंक्तियाँ इतनी प्रसिद्ध हो गयीं की इन्हे सहमति (कन्सेंट) केस के फरियादी (कंप्लेनेंट) के वक़ील ने अपने बयान में शामिल किया.
सहमति पर ये बातचीत नई नहीं है, बल्कि पिछली एक शताब्दी से चली आ रही है – चाहे वह सहमति की उम्र तय करने की बात रही हो या यौन हिंसा के दौरान सहमति की या व्यक्तिगत अधिकार व हक़ की. सहमति एक लैंगिक (gendered) मुद्दा है. एक पितृसत्तात्मक (patriarchal) व्यवस्था में एक औरत के शरीर से प्रतिष्ठा और मान जुड़ा जाता है. महिला अधिकार आंदोलन ने सहमति को अपने शरीर पर खुद के हक़ और मानवाधिकार के साथ समझा है.
यौन हिंसा और दुर्व्यवहार के फरियादी (कम्प्लेनेंट) से अब भी ये पूछा जाता है की उन्होंने साफ़ और स्पष्ट शब्दों में ना कहा था या नही. ये सवाल एक तरह से ये मान कर चलता है कि कम्प्लेनेंट ने शायद पूरी तरह ना नहीं कहा या अस्पष्ट ना कहा (feeble no). इसके पीछे कि सोच शायद लोकप्रिय संस्कृति या फिल्मी गानों के इस विचार से प्रभावित होती है, कि ‘लड़की कि ना में आधी हाँ होती है. इस तरह कि सोच और गानों को सुनते हम सब बड़े हुए है. ऐसी बातों का एक ही मतलब हुआ, कि आपकी सहमति के कोई मायने नहीं है. बहुत खूबसूरत लगने वाले इस तरह के गानों का सन्देश था कि किस तरह एक औरत के ख्यालों, शरीर, सोच और ज़िन्दगी पर अधिकार ही प्यार है. मैं शायद आपको ऐसे कुछ गाने बता सकती हूँ, पर मुझे पूरा अंदाज़ा है कि अब तक आप लोग ऐसे कुछ गाने सोच चुके होंगे जिन्हें आप कभी कभार गुनगुनाते होंगे लेकिन सोचें तो फिल्म में उन गानों में किसी के साथ यौन दुर्व्यवहार और बदतमीज़ी हो रही होगी. शायद हर उम्र कि औरतें आप को अपने ज़माने के ऐसे गानों कि एक लिस्ट दे सकती है.
जब आप इस पर बात करना चाहते हैं तो आपको याद दिलाया जाता है कि कि फिल्में, गाने सब बस मनोरंजन के लिए हैं और ये सिर्फ eve – teasing और छेड़छाड़ ही था, किसी का कोई नुकसान का कोई इरादा नहीं था. यहाँ फिर intent या सामने वाले इंसान का ‘इरादा ख़राब नहीं था ‘ पर बात आ जाती है, पर इस बात पर नहीं कि किस तरह किसी को – उनके शरीर और व्यक्तित्व को objectify किया जा रहा है. उनके अपनी शर्तों पर अपने शरीर पर अधिकार को, बल्कि किसी के मानवाधिकार को ही नाकारा जा रहा है. यहाँ एक औरत कि मर्ज़ी, अधिकार, स्वायत्तता, सहमति पर कोई ध्यान नहीं है. बल्कि सहमति पूछने कि बात तो इतनी अनोखी लगती है कि उस पर कहाँ ही बात कि जाती है, वहीं आज्ञाकारी होने को एक बहुत बड़ी अच्छाई माना जाता है. इस में अगर जेंडर भूमिका भी जोड़ दी जाए तो औरत को अपने शरीर पर कोई अधिकार रह ही नहीं जाता. पीछा करने वाले गानों को मनोरंजन मानना, यौन हिंसा को eve teasing कह कर टाल देना और ‘ boys will be boys ‘ जैसी बातें सिर्फ फिल्म के डायलाग नहीं रह जाते पर लगभग सब औरतों को कभी न कभी सुन ने पड़ते है. इस पर भी हैरानी कि बात ये है कि हम सभी उन लोगों को जानते हैं जिनके साथ यौन हिंसा या दुर्व्यवहार हुआ है, पर ऐसा करने वालों को नही.
#metoo आन्दोलन से सहमति पर होने वाली बातचीत में एक बहुत बदलाव आया है. साथ ही कुछ फिल्मों जैसे PINK इत्यादि भी आयीं जहाँ सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तरीके से औरत कि सहमति पर बात हो रही होती है. मुख्यधारा सिनेमा जो अधिक लोगों तक पहुँचता है, वो भी सहमति के भिन्न पहलुओं पर बात करने कि कोशिश कर रहा है, जहाँ औरत अपनी सहमति पर अपने फैसले और हक़ कि बात कर रही है ना कि परिवार, समाज और प्रतिष्ठा की.
सहमति से जुड़े एक और पहलू पर बात हो रही है – क्या सहमति या असहमति सिर्फ बोल कर ज़ाहिर की जा सकती है? संयुक्त राष्ट्र (United Nations) सहमति को उत्साहपूर्वक, बिना ज़ोर ज़बरदस्ती, सब जान ने के बाद दी गयी और बदली जा सकने वाली परिभाषित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सहमति दूसरे के द्वारा तय की गयीं सीमओं का सम्मान है, जिन्हें वे अपने लिए तय कर सकते हैं. इसलिए ‘ना का मतलब ना’ के साथ साथ इस बात पर भी ज़ोर दिया जाना चाहिए की किसी से स्वीकृति या सहमति या रज़ामंदी ज़बरदस्ती करके, अपनी ज़िद्द मनवाने के लिए या पूरे होशोहवास में न होते हुए, न ली जाए.
सहमति पर छोटी उम्र से ही बात की जानो चाहिए, बड़ों से भी जहाँ सहमति केवल यौन और शारीरिक तक ही सीमित नहीं है। सहमति माने दूसरे की अपने खुद के लिए तय की गयीं सीमाओं का उल्लंघन न करना, उन्हें अपने मुताबिक चीज़ें करने पर मजबूर न करना.
सहमति अपनी मर्ज़ी मुताबिक, उत्साहपूर्वक, बदली जाने योग्य और सम्मान की बात है।
स्वीकृति/ रज़ामंदी/ मर्ज़ी/ सहमति (कंसेंट) वो है जो
मन मुताबिक,
पूरे होशो हवास में
और उत्साहपूर्वक दी गयी.
वह कभी भी बदली जा सकती है.
स्वीकृति/ रज़ामंदी/ मर्ज़ी/ सहमति (कंसेंट) ये नहीं
ज़ोर ज़बरदस्ती
उनके मना करने के बाद भी बार बार अपनी बात कहके ज़बरदस्ती करते रहना
अपनी बात मनवाने की ज़िद्द
उन्हें ना कहने का मौका, अधिकार और हक़ न देना
दूसरे को अपने मुताबिक बर्ताव के लिए मजबूर करना
साथ ही
एक बार की हाँ का मतलब, हर बार हाँ नहीं है.
उनकी ना को मान लेना – चाहे वो शब्दों में हो या उनके बर्ताव से
उनकी मर्ज़ी की इज़्ज़त करना
अगर वो सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक न करें, उसे स्वीकार करना
अगर हाँ कहने के बाद भी वे अपना विचार बदल दें, उसे स्वीकार करना
ये मान और जान लेना कि अपने शरीर पर सभी को पूरा अधिकार और हक़ है